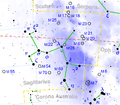शीर्ष प्रश्न
समयरेखा
चैट
परिप्रेक्ष्य
हिन्दू पंचांग
दिनांक गणना हेतु कैलेंडर विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश
Remove ads
पंचांग एक वैदिक ज्योतिषीय ग्रंथ है जो हिंदू धर्म और ज्योतिष में समय मापन और शुभ मुहूर्त निर्धारण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शब्द संस्कृत के "पंच" (पांच) और "अंग" (अंग या भाग) से बना है। जिसका अर्थ है पांच अंगो वाला , जो भारत में प्राचीन काल से परंपरागत रूप से उपयोग में लाए जाते रहे हैं। पञ्चाङ्ग में समय गणना के पाँच अंग हैं : वार , तिथि , नक्षत्र , योग , और करण। [1]
ये चान्द्रसौर प्रकृति के होते हैं। सभी हिन्दू पञ्चाङ्ग, कालगणना के एक समान सिद्धांतों और विधियों पर आधारित होते हैं किन्तु मासों के नाम, वर्ष का आरम्भ (वर्षप्रतिपदा) आदि की दृष्टि से अलग होते हैं।
भारत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पञ्चाङ्ग ये हैं-
- (१) विक्रमी पञ्चाङ्ग - यह सर्वाधिक प्रसिद्ध पञ्चाङ्ग है जो भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में प्रचलित है।
- (२) तमिल पञ्चाङ्ग - दक्षिण भारत में प्रचलित है,
- (३) बंगाली पञ्चाङ्ग - बंगाल तथा कुछ अन्य पूर्वी भागों में प्रचलित है।
- (४) मलयालम पञ्चाङ्ग - यह केरल में प्रचलित है और सौर पंचाग है।
हिन्दू पञ्चाङ्ग का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी भारत और नेपाल सहित कम्बोडिया, लाओस, थाईलैण्ड, बर्मा, श्री लंका आदि में भी प्रयुक्त होता है। हिन्दू पञ्चाङ्ग के अनुसार ही हिन्दुओं/बौद्धों/जैनों/सिखों के त्यौहार होली, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, वैशाखी, रक्षा बन्धन, पोंगल, ओणम ,रथ यात्रा, नवरात्रि, लक्ष्मी पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, रामनवमी, विसु और दीपावली आदि मनाए जाते हैं।
Remove ads
वार
सारांश
परिप्रेक्ष्य
भारतीय पंचांग प्रणाली में एक प्राकृतिक सौर दिन को दिवस कहा जाता है। सप्ताह में सात दिन होते हैं और उनको वार कहा जाता है। दिनों के नाम सूर्य , चन्द्र , और पांच प्रमुख ग्रहों पर आधारित हैं , हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है, जैसे रविवार का स्वामी सूर्य और सोमवार का स्वामी चंद्रमा है। दिन के स्वामी ग्रह के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए शुभता या अशुभता निर्धारित की जाती है। [1]
शनिवार के लिए थावर राजस्थानी और हरयाणवी में प्रचलित है। थावर को स्थावर का तद्भव माना जाता है। रविवार के लिए आदित्यवार के तद्भव आइत्तवार ,इत्तवार,इतवार अतवार , एतवार इत्यादि प्रचलित हैं।
Remove ads
काल गणना - घटि, पल, विपल
हिन्दू समय गणना में समय की अलग अलग माप इस प्रकार हैं। एक सूर्यादय से दूसरे सूर्योदय तक का समय दिवस है , एक दिवस में एक दिन और एक रात होते हैं। दिवस से आरम्भ करके समय को साठ साठ के भागों में विभाजित करके उनके नाम रखे गए हैं ।
१ दिवस = ६० घटी (६० घटि २४ घंटे के बराबर है या १ घटी = २४ मिनट , घटि को देशज भाषा में घडी भी कहा जाता है )
१ घटी = ६० पल (६० पल २४ मिनट के बराबर है या १ पल = २४ सेकेण्ड)
१ पल = ६० विपल (६० विपल २४ सेकेण्ड के बराबर है , १ विपल = ०.४ सेकेण्ड)
१ विपल = ६० प्रतिविपल [1]
इसके अतिरिक्त
१ पल = ६ प्राण ( १ प्राण = ४ सेकेण्ड )
इस प्रकार एक दिवस में ३६०० पल होते हैं। एक दिवस में जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसके कारण सूर्य विपरीत दिशा में घूमता प्रतीत होता है। ३६०० पलों में सूर्य एक चक्कर पूरा करता है , इस प्रकार ३६०० पलों में ३६० अंश। १० पल में सूर्य का जितना कोण बदलता है उसे १ अंश कहते है।
Remove ads
तिथि, पक्ष और माह
सारांश
परिप्रेक्ष्य
हिन्दू पंचांगों में मास, माह व महीना चन्द्रमा के अनुसार होता है। अलग अलग दिन पृथ्वी से देखने पर चन्द्रमा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जिस दिन चन्द्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के उपरांत चन्द्रमा घटने लगता है और अमावस्या तक घटता रहता है। अमावस्या के दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं देता और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लगभग चौदह व पन्द्रह दिनों में बढ़कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार चन्द्रमा के चक्र के दो भाग है। एक भाग में चन्द्रमा पूर्णिमा के उपरांत अमावस्या तक घटता है , इस भाग को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस पक्ष में रात के आरम्भ मे चाँदनी नहीं होती है। अमावस्या के उपरांत चन्द्रमा बढ़ने लगता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को शुक्ल पक्ष कहते हैं। पक्ष को साधारण भाषा में पखवाड़ा भी कहा जाता है। चन्द्रमा का यह चक्र जो लगभग २९.५ दिनों का है चंद्रमास व चन्द्रमा का महीना कहलाता है । दूसरे शब्दों में एक पूर्ण चन्द्रमा वाली स्थिति से अगली पूर्ण चन्द्रमा वाली स्थिति में २९.५ का अन्तर होता है।[1]
चंद्रमास २९.५ दिवस का है , ये समय तीस दिवस से कुछ ही घटकर है। इस समय के तीसवें भाग को तिथि कहते हैं। इस प्रकार एक तिथि एक दिन से कुछ मिनट घटकर होती है। पूर्ण चन्द्रमा की स्थिति (जिसमे स्थिति में चन्द्रमा सम्पूर्ण दिखाई देता हो ) आते ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है और कृष्ण पक्ष की पहली तिथि आरम्भ हो जाती है। दोनों पक्षों में तिथियाँ एक से चौदह तक बढ़ती हैं और पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात पंद्रहवी तिथि पूर्णिमा व अमावस्या होती है।
तिथियों के नाम निम्न हैं- पूर्णिमा (पूरनमासी), प्रतिपदा (पड़वा), द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), पंचमी (पंचमी), षष्ठी (छठ), सप्तमी (सातम), अष्टमी (आठम), नवमी (नौमी), दशमी (दसम), एकादशी (ग्यारस), द्वादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस), चतुर्दशी (चौदस) और अमावस्या (अमावस)।
तिथियों के प्रकार निम्न हैं- शुक्ल व कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, षष्ठी व एकादशी तिथि को नंदा तिथि, द्वितीय, सप्तमी व द्वादशी तिथि को भद्र तिथि, तृतीय, अष्टमी व त्रयोदशी तिथि को जया तिथि, चतुर्थी, नवमी, पूर्णिमा या अमावस्या तिथि को रिक्त तिथि के नाम से जाना जाता है।[4]
माह के अंत के दो प्रचलन है। कुछ स्थानों पर पूर्णिमा से माह का अंत करते हैं और कुछ स्थानों पर अमावस्या से। पूर्णिमा से अंत होने वाले माह पूर्णिमांत कहलाते हैं और अमावस्या से अंत होने वाले माह अमावस्यांत कहलाते हैं। अधिकांश स्थानों पर पूर्णिमांत माह का ही प्रचलन है। चन्द्रमा के पूर्ण होने की सटीक स्थिति सामान्य दिन के बीच में भी हो सकती है और इस प्रकार अगली तिथि का आरम्भ दिन के बीच से ही सकता है। [1]
Remove ads
नक्षत्र
सारांश
परिप्रेक्ष्य
तारामंडल में चन्द्रमा के पथ को २७ भागों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा गया है। दूसरे शब्दों में चन्द्रमा के पथ पर तारामंडल का १३ अंश २०' का एक भाग नक्षत्र है। [1] हर भाग को उसके तारों को जोड़कर बनाई गई एक काल्पनिक आकृति के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक नक्षत्र का अपना ज्योतिषीय प्रभाव होता है, जो उस दिन के कार्यों को प्रभावित कर सकता है।[5]
Remove ads
योग और करण
चन्द्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर दूरी (कोण) तय करते हैं उसे योग कहते हैं, क्योंकि ये चन्द्रमा और सूर्य की दूरी का योग है । ज्योतिष में ग्रहों की विशेष स्थितियों को भी योग कहा जाता है वह एक भिन्न विषय है। एक तिथि का आधा समय करण है।
चन्द्रमास और ग्रहण
सूर्य और चंद्र ग्रहण का सम्बन्ध सूर्य और चन्द्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों से है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही आरम्भ होते है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही आरम्भ होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की सहायता से अमावस्या तिथि के अंत को समझना सरल है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का आरम्भ अमावस्या तिथि में होता है , जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है तब अमावस्या तिथि का अंत होता है और उसके बाद अगली तिथि आरम्भ हो जाती है जिसमे सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। दो सूर्य ग्रहणों या दो चंद्र ग्रहणों के बीच का समय एक या छह चंद्रमास हो सकता हैं। ग्रहणों के समय का अध्ययन चंद्रमासों में करना सरल है क्योकि ग्रहणों के बीच की अवधि को चंद्रमासों में पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है
Remove ads
महीनों के नाम
सारांश
परिप्रेक्ष्य
इन बारह मासों के नाम आकाशमण्डल के नक्षत्रों में से १२ नक्षत्रों के नामों पर रखे गये हैं। जिस मास जो नक्षत्र आकाश में प्रायः रात्रि के आरम्भ से अन्त तक दिखाई देता है या कह सकते हैं कि जिस मास की पूर्णमासी को चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम पर उस मास का नाम रखा गया है। चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र मास (मार्च-अप्रैल), विशाखा नक्षत्र के नाम पर वैशाख मास (अप्रैल-मई), ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ मास (मई-जून), आषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर आषाढ़ मास (जून-जुलाई), श्रवण नक्षत्र के नाम पर श्रावण मास (जुलाई-अगस्त), भाद्रपद (भाद्रा) नक्षत्र के नाम पर भाद्रपद मास (अगस्त-सितम्बर), अश्विनी के नाम पर आश्विन मास (सितम्बर-अक्टूबर), कृत्तिका के नाम पर कार्तिक मास (अक्टूबर-नवम्बर), मृगशीर्ष के नाम पर मार्गशीर्ष (नवम्बर-दिसम्बर), पुष्य के नाम पर पौष (दिसम्बर-जनवरी), मघा के नाम पर माघ (जनवरी-फरवरी) तथा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन मास (फरवरी-मार्च) का नामकरण हुआ है। [6][7]
Remove ads
1996
सारांश
परिप्रेक्ष्य
Saptami tithi

आमतौर पर प्रचलित भारतीय वर्ष गणना प्रणालियों में प्रत्येक को सम्वत कहा जाता है। हिन्दू , बौद्ध , और जैन परम्पराओं में कई सम्वत प्रचलित हैं जिसमे विक्रमी सम्वत , शक संवत् , प्राचीन शक संवत् प्रसिद्ध हैं। [11]
हिन्दी वार्तालाप में गैर भारतीय प्रणालियों के लिए भी संवत् शब्द का प्रयोग हो सकता है । हर संवत् में वर्तमान वर्ष का अंक ये बताता है कि सम्वत शुरू हुए कितने वर्ष हुए हैं । जैसे विश्व भर में प्रचलित ईस्वी संवत् का ये 2025 वर्ष है। हिन्दू त्यौहार हिन्दू पंचाग के अनुसार होते हैं। हिन्दू पंचांगों में की संवत् प्रचलित हैं , जिनमे हिंदी भाषी क्षेत्रों में विक्रम संवत् प्रचलित है। विक्रम संवत् का आरम्भ मार्च या अप्रेल में होता है। इस वर्ष लगभग मार्च/अप्रैल 2025 से फरवरी/मार्च 2026 तक विक्रमी सम्वत 2082 है। [12]
संवत् या तो कार्तिक कृष्ण पक्ष से आरम्भ होते हैं या चैत्र कृष्ण पक्ष से। कार्तिक से आरम्भ होने वाले संवत् को कर्तक संवत् कहते हैं। संवत् में अमावस्या को अंत होने वाले माह (अमावस्यांत माह ) या पूर्णिमा को अंत होने वाले माह (पूर्णिमांत) माह कहा जाता है। किसी संवत् में पूर्णिमांत माह का प्रयोग होता है और किसी में अमावस्यांत का। भारत के अलग अलग स्थानों पर एक ही नाम की संवत् परम्परा में पूर्णिमांत या अमावस्यांत माह का प्रयोग हो सकता है। विक्रम संवत् का आरम्भ चैत्र माह के कृष्ण पक्ष से होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष दिवाली से आरम्भ होता है , इस दिन से वर्ष का आरंभ होने वाले संवत् को विक्रम संवत् (कर्तक ) कहा जाता है।
संवत् के अनुसार एक वर्ष की अवधि को भी संवत् कहा जा सकता है , जैसे:- संवत् १६८० में तुलसीदास जी की मृत्यु हुई।
Remove ads
इन्हे भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
सन्दर्भ
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads